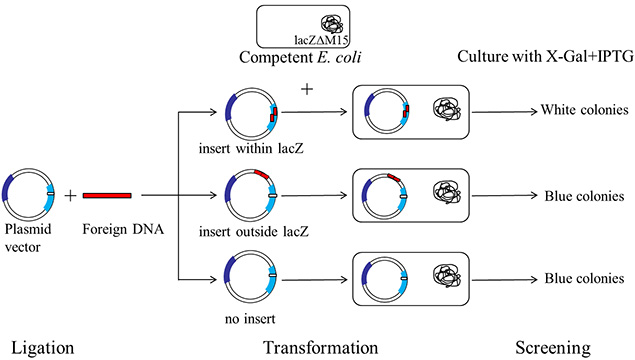Jharkhand Ki Janjatiya
➧ झारखंड में जनजातियों का अधिवास पुरापाषाण काल से ही रहा है।
➧ विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है।
➧ झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति एवं गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है।
➧ आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ 'आदि काल से रहने वाले लोग' हैं।
➧ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है।
➧ झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजातियां क्रमश: संथाल, उरांव, मुंडा और हो हैं ।
➧ झारखंड में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आते हैं। शेष 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है जिसमें बिरहोर, कोरवा, असुर, पहरिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरजिया तथा सबर शामिल हैं ।
➧ आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि पूर्वकालीन है तथा इसका जीवन-यापन आखेट, शिकार और झूम कृषि पर आधारित है।
➧ झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है।
➧ मुंडा जनजाति के बारे में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया।
➧ झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का अहम योगदान रहा है।
➧ उराँव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटानागपुर प्रदेश में आए। इनकी एक शाखा राजमहल क्षेत्र में जबकि दूसरी शाखा पलामू क्षेत्र में बस गयी ।
➧ झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका की बेड्डा तथा आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से साम्यता रखते हैं।
➧ झारखंड के आदिवासी प्रोटो-आस्ट्रोलॉयड प्रजाति से संबंध रखते हैं।
➧ जॉर्ज ग्रियर्सन (भाषा वैज्ञानिक) ने झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को ऑस्ट्रिक एवं द्रविड़ दो समूह में विभाजित किया है।
➧ भाषायी आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार तथा द्रविड़ियन/द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार का संबंध आस्ट्रिक महाभाषा परिवार से है।
➧ आस्ट्रिक महाभाषा परिवार के अंतर्गत ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के अलावा ऑस्ट्रोनिशियन भाषा परिवार (दक्षिण-पूर्व एशिया) शामिल है
➧ द्रविड़ भाषा परिवार बोलने वाली अधिक जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवास करती हैं
➧ भाषायी विविधता के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध 'कुड़ुख' भाषा से है, जबकि माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया जनजाति 'मालतो भाषा' (द्रविड़ समूह की भाषा) से संबंधित है। शेष जनजातियों का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा समूह से है।
➧ 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या का 26.2% है।
➧ झारखंड की कुल जनजातीय आबादी को लगभग 91% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 9% शहरी क्षेत्र में निवास करती हैं।
➧ झारखंड का जनजातीय समाज मुख्यत: पितृसत्तात्मक है।
➧ झारखंड की जनजातियों में प्रया: एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है।
➧ झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद की इजाजत नहीं होती है।
➧ यहां की जनजातियों में विभिन्न गोत्र पाए जाते हैं। गोत्र को किली, कुंदा, पारी आदि नामों से जाना जाता है।
➧ जनजातियों के प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक/ गोत्रचिन्ह होता है, जिससे टोटम कहा जाता है।
➧ प्रत्येक गोत्र से एक प्रतीक/गोत्रचिन्ह (प्राणी, वृक्ष या पदार्थ) संबंधित होता है, जिसे हानि पहुंचाना या इसका प्रयोग सामाजिक नियमों द्वारा वर्जित होता है।
➧ जनजातियों के प्रत्येक गोत्र अपने-आप को एक विशिष्ट पूर्वज की संतान मानते हैं।
➧ पहाड़िया जनजाति में गोत्र की व्यवस्था नहीं पाई जाती है।
➧ जनजातियों में समगोत्रीय में विवाह निषिद्ध होता है।
➧ विवाह पूर्व सगाई की रस्म केवल बंजारा जनजाति में ही प्रचलित है।
➧ सभी जनजातियों में वैवाहिक रस्म-रिवाज में सिंदूर लगाने की प्रथा है। केवल खोंड जनजाति में जयमाला की प्रथा प्रचलित है।
➧ जनजातियों में विवाद संबंधी कर्मकांड पुजारी द्वारा संपन्न कराया जाता है जिन्हें पाहन, देउरी आदि कहा जाता है। कुछ जनजातियों में ब्राह्मण द्वारा भी संपन्न कराया जाता है।
➧ झारखण्ड की जनजातियों में सामान्यतः बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है।
➧झारखण्ड की जनजातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह इस प्रकार हैं।
क्रय विवाह : संथाल, उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर, कवर।
सेवा विवाह : संथाल, उरांव, मुंडा , बिरहोर, कवर, भूमिज ।
विनिमय विवाह : झारखण्ड की लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है।
हठ विवाह : संथाल, हो , मुंडा , बिरहोर।
हरण विवाह : उरांव, हो, खड़िया, बिरहोर, भूमिज, मुंडा , सौरिया पहाड़िया।
सह-पलायन विवाह: मुंडा , खड़िया, बिरहोर।
विधवा विवाह : संथाल, उरांव, मुंडा , बिरहोर, बंजारा।
➧ झारखंड की जनजाति में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख संस्थाएं अखड़ा (पंचायत स्थल/नृत्य का मैदान), सरना (पूजा स्थल) एवं युवागृह (शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु संस्था) आदि है।
➧ ताना भगत तथा साफाहोड़ (सिंगबोंगा के प्रति निष्ठा रखने वाले) समूहों को छोड़कर शेष जनजातीय समाज प्राय: मांसाहारी होते हैं।
➧ जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है जिसमें प्रकृति पूजा की जाती है।
➧ जनजातियों के पर्व-त्यौहार सामान्यत: कृषि एवं प्रकृति से संबंधित होते हैं।
➧ झारखंड की अधिकांश जनजातियों के प्रमुख देवता सूर्य हैं। जिन्हें विभिन्न जनजातियों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है।
➧ जनजातीय समाज में मृत्यु के बाद शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। इसाई, उरांव में शवों को अनिवार्यता: दफनाया जाता है।
➧ झारखण्ड की जनजातियों का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि कार्य है। इसके अतिरिक्त जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन, पशुओं का शिकार, वनोत्पादों का संग्रह, शिल्पकारी कार्य व मजदूरी जैसी गतिविधियां भी अपनाते हैं।
➧ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री हेतु यहां की जनजातियों में हाट का महत्वपूर्ण स्थान है।
➧ राज्य की तुरी जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं तथा उस घर में पहुंचते हैं जहां हाल ही में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या एक शिशु का जन्म हुआ हो।
➧ यह जनजाति अपने घरों की नर्म, गीली मिट्टी को पेंट करने के लिए अपनी उंगलियों का प्रयोग करती हैं ये अपने घरों की सजावट पौधों और पशु प्रजनन स्वरूपों में करते हैं।
👉 Previous Page:Jharkhand Ki Janjatiya Shasan Vyavastha Part-2
👉 Next Page:उरांव जनजाति का सामान्य परिचय